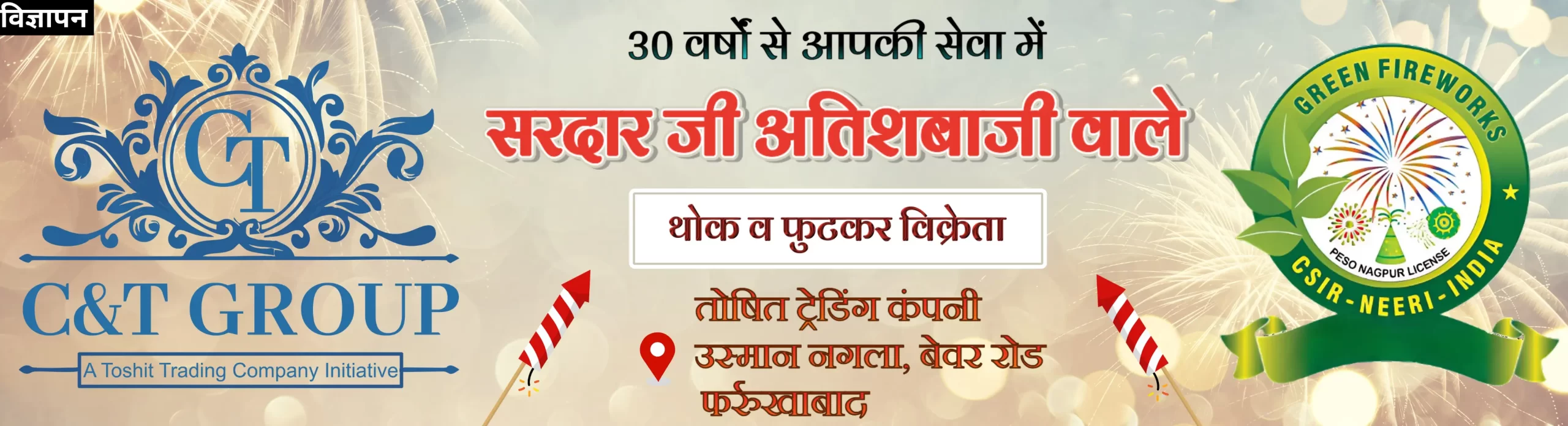23 मार्च का दिन भारत के लिए एक विशिष्टता रखता है| इस दिन डा.राममनोहर लोहिया का जन्म दिवस और भगतसिंह का शहादत दिवस है। यह जन्म और शहादत का एक अद्भुत संयोग है क्योंकि इन दोनों महानुभावों के मध्य एक अजीब सा अंतर्संबंध देखने को मिलता है|
 दोनों का ही जन्म ऐसे परिवारों में हुआ जिनका आज़ादी के संघर्ष में बड़ा योगदान रहा। भगतसिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और उनके पिता सरदार किशन सिंह भी स्वातंत्र्य संग्राम से जुड़े हुए थे। अल्प आयु में ही भगत सिंह खेत में बंदूकें बोते दिखाई देते हैं जिससे एक ऐसी फसल तैयार कर सके अंग्रेज देश से भाग जाएँ| 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के शहीदों की माटी को भगत सिंह कांच की शीशी में भर लाए थे और उसको हाथ में रख यह कसम खाई थी की उन शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जायेगी| वहीँ डा.राममनोहर लोहिया के पिता हीरालाल नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे और पेशे से अध्यापक होने के साथ हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यह संस्कार उन्होंने बालक राममनोहर को सहज ही प्रदान किया| ‘होनहार बीरवान के होत चीकने पात’ को सत्य सिद्ध करते हुए बाल्यकाल में ही लोहिया ने लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली अगस्त को हड़ताल की और गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में ही स्कूल त्याग दिया। गांधी के आह्वान पर स्कूल त्याग असहयोग आंदोलन में भगत सिंह भी पूरी तत्परता से कूदे थे| इस प्रकार हम देखते हैं की भगत सिंह और लोहिया, दोनों में ही बचपन से ही राष्ट्रप्रेम का जन्म होता है और दोनों ही क्रान्ति के मार्ग को अपनाने का संकल्प लेते हैं|
दोनों का ही जन्म ऐसे परिवारों में हुआ जिनका आज़ादी के संघर्ष में बड़ा योगदान रहा। भगतसिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और उनके पिता सरदार किशन सिंह भी स्वातंत्र्य संग्राम से जुड़े हुए थे। अल्प आयु में ही भगत सिंह खेत में बंदूकें बोते दिखाई देते हैं जिससे एक ऐसी फसल तैयार कर सके अंग्रेज देश से भाग जाएँ| 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला के शहीदों की माटी को भगत सिंह कांच की शीशी में भर लाए थे और उसको हाथ में रख यह कसम खाई थी की उन शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जायेगी| वहीँ डा.राममनोहर लोहिया के पिता हीरालाल नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे और पेशे से अध्यापक होने के साथ हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यह संस्कार उन्होंने बालक राममनोहर को सहज ही प्रदान किया| ‘होनहार बीरवान के होत चीकने पात’ को सत्य सिद्ध करते हुए बाल्यकाल में ही लोहिया ने लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली अगस्त को हड़ताल की और गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में ही स्कूल त्याग दिया। गांधी के आह्वान पर स्कूल त्याग असहयोग आंदोलन में भगत सिंह भी पूरी तत्परता से कूदे थे| इस प्रकार हम देखते हैं की भगत सिंह और लोहिया, दोनों में ही बचपन से ही राष्ट्रप्रेम का जन्म होता है और दोनों ही क्रान्ति के मार्ग को अपनाने का संकल्प लेते हैं|
भगत सिंह अपने कॉलेज जीवन से ही विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों से संबद्ध रहे| कीर्ति किसान पार्टी के कार्यकर्ता और नौजवान भारत सभा के कुशल संचालक रहे| लोहिया भी 1924 में एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए थे। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने खद्दर पहनना शुरू कर दिया था। 1926 में पिताजी के साथ गौहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए। यही नहीं, अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाषचंद्र बोस के न पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। 1928 में कलकता में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। 1928 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में भी सक्रिय हुए। साइमन कमिशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया। कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तथा सुभाषचंद्र बोस और लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए। गौरतलब है कि साइमन कमीशन के खिलाफ भगत सिंह ने भी प्रखर आंदोलन किया था|
भगतसिंह अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और अध्ययनशील थे। दस वर्ष की उम्र में ही भगत सिंह ने बाबा सूफी प्रसाद, अम्बा प्रसाद और लाला हरदयाल व अन्य निर्वासित या फरार क्रांतिकारियों का साहित्य पढ़ लिया था| लोहिया भी बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के रहे। अपने बर्लिन प्रवास के दौरान उन्होंने जर्मन भाषा को मात्र तीन महानों मे सीख लिया था| यहाँ तक की उनके प्रोफसर जोम्बार्ट भी इस बात से अत्यंत चकित थे।
हम इन दोनों क्रांतिकारियों में यह भी साम्य पाते हैं की दोनों ही समाजवाद के पक्षधर थे| भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समाजवाद के सिद्धांतों को शामिल करने वाले क्रांतिकारी बने| लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित “द्वारकादास पुस्तकालय” उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों और बैठकों का प्रमुख केंद्र था| पुस्तकालय के तात्कालिक अध्यक्ष श्री राजाराम शास्त्री के शब्दों में वहाँ होने वाली बहसों के दौरान सरदार भगत सिंह उग्र और सशस्त्र क्रान्ति के साथ ही समाजवाद का भी खुला समर्थन करते थे| कार्ल-मार्क्स से पूरी तरह प्रभावित होने के साथ ही वे प्रसिद्ध रूसी अराजकतावादी बाकुनिन के भी प्रशंसक थे| अपने क्रांतिकारी दल ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी’ को भगत सिंह ने ही प्रेरणा दी कि वह अपना उद्देश्य देश की संपूर्ण आजादी हासिल करने के साथ ही साथ एक आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना भी घोषित करे। उनके प्रयासों से ही क्रांतिकारी दल के नाम के साथ ‘सोशलिस्ट’ शब्द जोड़ा गया।
डा. राममनोहर लोहिया ने भी सदा आदर्श समाजवाद की ही वकालत की और देश के आज़ाद होने के बाद भी किसान मजदूरों का एक ‘सार्वभौमिक समाजवादी राज्य’ स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। लोहिया ने मार्क्सवाद और गांधीवाद को पूर्ण रूप से समझा और दोनों को ही अधूरा पाया| कारण, इतिहास की गति ने दोनों को छोड़ दिया| लोहिया ने माना की दोनों का महत्व युगानुसार ही है| उन्होंने माना की मार्क्स पश्चिम के और गांधी पूर्व के प्रतीक हैं| लोहिया इस पश्चिम-पूर्व की खाई पाटना चाहते थे और वस्तुत: अमीर-गरीब, बड़े-छोटे देश, काले-गोरे, पूर्व-पश्चिम और नर-नारी के बीच की असमानता समाप्त करना चाहते थे| यही उनका भारतीय समाजवाद था|
सन् 1934 में अंजुमन ए इस्लामिया हाल, पटना में ‘कांग्रेस समाजवादी पार्टी’ की जब आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापना हुई तो राममनोहर लोहिया ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई। डा. लोहिया ने उस कार्यक्रम में समाजवादी आंदोलन की भावी रुपरेखा पेश की थी।
इन दोनों ही की आत्मा विद्रोही थी| अन्याय का प्रतिकार दोनों के ही सिद्धांतों और कर्मों की बुनियाद रहा| भगत सिंह ने सदा ही सिद्धांतयुक्त क्रान्ति की पैरवी की| उन्होंने कहा था: “मैंने एक आतंकवादी तरह अपने क्रांतिकारी जीवन के प्रारम्भिक काल में कार्य किया| किन्तु वस्तुत: मैं एक आतंकवादी नहीं हूँ बल्कि एक ऐसा क्रांतिकारी हूँ, जिसके पास सुनिश्चित विचार हैं और एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है।’ वहीँ लोहिया ने भी महायुद्ध के समय युद्धभर्ती का विरोध, देशी रियासतों में आंदोलन, ब्रिटिश माल जहाजों से माल उतारने व लादने वाले मजदूरों का संगठन तथा युद्धकर्ज को मंजूर तथा अदा न करने, जैसे चार सूत्रीय मुद्दों को लेकर युद्ध विरोधी प्रचार किया था। ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह के विशाल जन क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता का भगत सिंह ने समर्थन किया था, उसकी झलक भी काफी हद तक सन् 1942 के क्रांतिकारी आंदोलन में डा. लोहिया की भूमिका में भी दिखती है।
भगत सिंह और उनके साथी जहां एक तरफ साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए तत्पर रहे, वहीं समाज की सड़ी-गली रुढियों, अंधविश्वासों और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी खूब संघर्ष करते रहे| सन 1925-26 में जब एक घोर साम्प्रदायिक हवा ने देश की फिजा को ढक लिया और जब बड़े-बड़े नेता भी इस साम्प्रदायिकता के प्रभाव में आ गए थे, भगत सिंह और उनकी टीम जगह जगह पर नाटकों और चर्चा-बैठकों के माध्यम से साम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान में प्रयासरत रही| हम इस दिशा में लोहिया का भी अद्भुत प्रयास देखते हैं| 1946-47 के संक्रान्ति-काल में साम्प्रदायिक शक्तियों को रोकने का सराहनीय प्रयास लोहिया द्वारा हुआ| उन्होंने 30 दिसंबर, 1946 को नवाखली में हिन्दु और मुसलमान के बीच के टकराव को दूर करने के लिए गांधी जी के साथ विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। पूरे साल नवाखली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर साम्प्रदायिकता की आग को बुझाने की कोशिश करते रहे। 14 अगस्त 1947 की रात को हिन्दु-मुस्लिम भाई-भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभा की। जब 31 अगस्त को वातावरण फिर बिगड़ गया और गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब लोहिया ने ही दंगाईयों के हथियार इकट्ठे कराए। लोहिया के प्रयासों से ही से शांति समिति की स्थापना हुई तथा 4 सितम्बर को गांधी जी ने अनशन तोड़ा।
हम भगत सिंह और लोहिया, दोनों में ही स्वभाषा के प्रति प्रेम का भाव देखते हैं| 17 वर्ष की कम उम्र में ही भगतसिंह को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ‘पंजाब में भाषा और लिपि की समस्या’ विषय पर एक पत्रिका के लेख पर 50 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला| उन्होंने 1924 में लिखा था कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी नहीं देवनागरी होनी चाहिए| उनका मानना था की यदि एक भाषा नहीं की जा सकती तो कम से कम एक लिपि तो अवश्य ही बनाई जा सकती है| इससे देश में ऐक्य बढ़ेगा| कुछ ऐसा ही भाव हम लोहिया में भी देखते हैं| अपने इतिहास और अपनी भाषा के संदर्भ में वे पश्चिम से कोई सिद्धांत उधार लेकर व्याख्या करने को बिलकुल राजी नहीं थे। सन् 1932 में जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले राममनोहर लोहिया ने साठ के दशक में देश से अंग्रेजी हटाने का जो आह्वान किया, उसकी गिनती अब तक के कुछ गिने-चुने आंदोलनों में की जा सकती है। उनके लिए स्वभाषा का समर्थन कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान का प्रश्न था और लाखों–करोडों को हीन भावनाओं से मुक्त हो आत्मविश्वास से भर देने का एक माध्यम था| लोहिया ने कहा था, ‘‘मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके मां बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हैं।’’
निश्चय ही इन दोनों के विचार, व्यवहार, योजना, दृष्टिकोण और कार्यपद्धिती का परस्पर साम्य अनुकरणीय है और आज जन्म और शहादत के संयोग के इस अवसर पर हम सभी भारतवासी इन दोनों को नमन करते हैं और इनके विचारों का अनुसरण करने का अहद उठाते हैं|